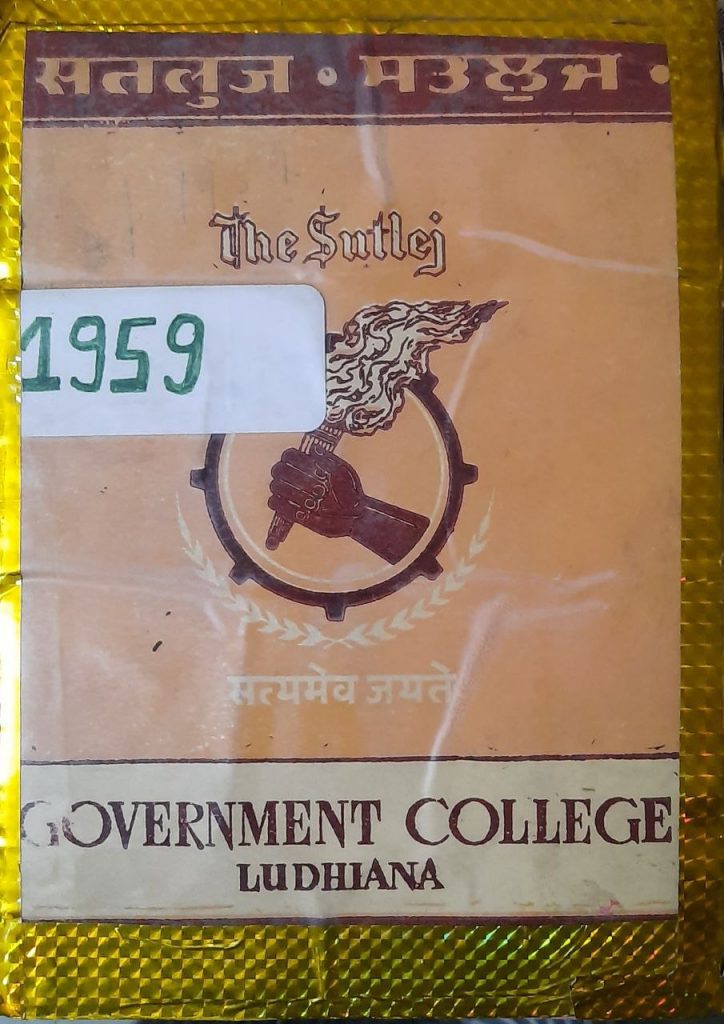साहित्य का सृजन -श्रीनिवास (1959 के दौर का एक प्रोफेसर श्रीनिवास का कॉलेज पत्रिका में एक संस्करण)
सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज अभिन्न अंग है। यही कारण है कि वह कृति-सूजन में व्यष्टि होता हुआ भी समष्टि है। कला सूजन के मूल में अपने व्यक्तित्व की छाप लिये वह ‘अथ’ से ‘इति’ तक चला जाता है।
वह व्यक्तित्व वायवी उपहार के रूप में अथवा काकतालीय फल के रूप में उसे नहीं मिला अपितु राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ ही हैं जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण विवेकिनी बुद्धि का निर्माण होता है। भाव इसी बुद्धि के अन्तर्गत हैं। भाव और बुद्धि संतुलित होकर जब भाषागत अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं तो उत्तम साहित्य का सृजन हुआ करता है। मनुष्य सामाजिक मान्यताओं से जकड़ा हुआ काला है फिर भी उसके व्यक्तित्व का राजपट स्वीकृति मौर विरोध के कौशेय सूत्रों से बुना है। साहित्य कार चाहे उद्धत होकर समाज की अवहेलना ही क्यों न कर दे पुनरपि अपरोक्ष रूप से उसके लिये सरणि का निदर्शन तो समाज हो करेगा । साहित्य में व्यक्ति और समाज का संघर्ष कोई नयी बात नहीं। वह विवेकशील है अतः प्रत्येक बात पर अंगीकारभंगी नहीं हो सकता। बात को खनका कर खरा करना उसे भली भान्ति आता है।
साहित्य का सम्बन्ध मानव जीवन से है इसीलिये कलाकार की पकड़ जीवन से सम्बद्ध घटनाओं में होने वाले भावों को धोर होती है। भावों से सम्बन्ध रखने के कारण ही किसी प्रकार का साहित्य कल्पना से शून्य नहीं हुआ करता । कल्पना से अभिप्राय वायवी किलों का ही संकलन मात्र नहीं बल्कि उसका सम्बन्ध जगत्-समाज से है। जैसे स्वर्ग में हिलोरें लेने वाली मन्दाकिनी वसुन्धरा के पापों को दूर करने को वसुधा पर अवतरित हुई थी वैसे ही व्यक्तिगत मानस के स्वर्ग से निकल कर साहित्य की गंगा समाज के ठोस धरातल की ओर बहती है। समाज की समस्याओं का ही आधार बना कर साहित्य-कार साहित्य-सृष्टि किया करता है-यहीं तो कारण है साहित्य को जीवन की आलोचना कहा गया है। कलाकार की सफलता के कारण हैं जीवन के सात्विक रूप को सम्मुख रखना और ऊंचे एवं स्थायी आदर्शों को उपस्थित करना ।
यही सात्विक रूप एवं स्थायी आदर्शों का मेल मणिकाञ्चन के संयोग के श्रादर्श को हमारे सामने लाता है। किसी भी काल का साहित्य देशविशेष एवं कालविशेष की तत्कालीन जनता-जनार्दन की चित्तवृत्ति का बिम्ब होता है। अमुककाल के लेखक का मूल्यांकन करते समय हमें तदनुरूप परिस्थितियों को टटोलना होगा । प्रवृत्तियों में परिवर्तन होने के कारण हम प्राचीन साहित्य एवं अर्वाचीन साहित्व को पृथक् तो कर सकते है परन्तु इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध अटूट है। नवीन के आगमन पर प्राचीन की गरिमा न्यून नहीं हुआ करती । कालीदास ने भी मालविकाग्नि-मित्र नाटक की प्रस्तावना में कहा था, “पुराण-मित्येव न साधुसर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्” । प्राचीन आदर्श ही तो नवीन श्रादर्श निर्धारित किया करते हैं। ऐसे ही श्राधुनिक युग पर विचार करतै समय रीतिकालीन कवियों की बिगर्हणा करनी अनुपयुक्त होगी। उसकाल की परिस्थितियों ने ही उन्हें ऐसा होने को विवश किया ।
साहित्य हितैषिता का सूत्र ग्रहण किये है। इसमें मनुष्य के अनुभव सन्निहित है । उच्चावच्छ स्थलों का प्रदर्शन कराने का आशय ही यही है। कि अमुक स्थिति कहां तक मानव हित की साधका अथवा बाधक है। प्राचीन संस्कृति की झलक तथ गौरव की स्मृति करवाना एवं उस गरिमा के नवीन युग में अवतरित करना उसके उद्देश्यों में से एक है। जिस से तामस वृत्तियों को उत्तेजना मिले मनुष्य अकर्मण्य होकर भ्रान्तियों और सम्देहों व ग्रस्त हो वह सत्साहित्य नहीं कहला सकता ।
आजकल तो साहित्य भण्डार उत्तरोत्तर वृद्धि पा रहा है। अगणित रचनाएँ छापेखाने उगल रहे हैं । इनमें से अधिकतर रचनाओं में सन और मस्तिष्क का धुआँ, भावों का कुहासा ही उपलब्ध होता है । उत्तम साहित्य के लिये साधना का जीवन अपेक्षित है । साहित्यकार को पहिले साधक होना चाहिये तब लेखनी उठानी चाहिये अन्यथा रचना सतही स्तर की होगी । साहित्य जीवन शक्ति का प्रमाण है- यह शक्ति उच्छृंखल रूप में भी अभिव्यक्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में यह समाज में विकार ही फैलाएगी । हमारा, कर्तव्य है कि इस शक्ति को प्रथम सिद्ध कर लिया जाए। इसके सिद्ध होने पर जिस साहित्य का सृजन होगा वह मानव-कल्याण के विधायक साधनों में अग्रगण्य होगा ।
सम्पादक : श्रीनिवास
साहित्य का सृजन -श्रीनिवास (1959 के दौर का एक प्रोफेसर का कॉलेज पत्रिका में एक संस्करण) यह सुंदर लेखन गवर्नमेंट कॉलेज, लुधियाना (अब सतीश चंदर धवन गवर्नमेंट कॉलेज, लुधियाना) की इनहाउस पत्रिका द सतलज से लिया गया है। कॉलेज लाइब्रेरियन को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे फटे हुए पन्नों से लेख सुरक्षित रखने की अनुमति दी। https://theglobaltalk.com/